
राष्ट्र की बात: मीडिया की स्वतंत्रता और सरकार की मंशा
नई दिल्ली, 15 अप्रैल: बीते 50 साल से अधिक अवधि में देश में तीन ताकतवर प्रधानमंत्री हुए जिनके पास बहुमत था और जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। पहली थीं इंदिरा गांधी जिन्होंने मार्च 1971 की शानदार जीत के बाद अपना कार्यकाल पूरा किया। दूसरे थे राजीव गांधी जो सन 1984 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए। तीसरे हैं नरेंद्र मोदी जो बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के पांचवें वर्ष में प्रवेश करने ही वाले हैं। जरा विचार कीजिए, क्या आप इन तीनों के नेतृत्व वाली सरकारों में कुछ समानता पाते हैं। मैं आपको संकेत देता हूं। जरा इस बारे में सोचिए कि आखिर इन तीनों ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में क्या किया? अगर आप इस संकेत के बाद भी अंदाजा नहीं लगा पाए तो दूसरा संकेत मौजूद है- आप इस विषय पर एक पत्रकार की तरह सोचिए। सच यह है कि इन तीनों ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में मीडिया को निशाना बनाया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल का पांचवां वर्ष शुरू होते ही सेंसरशिप लागू कर दी। बाद में उन्होंने सदन का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया। उनकी दलील थी कि मीडिया नकारात्मक खबरें फैला रहा है और वह निहित स्वार्थ वाले तत्त्वों से संचालित है। उन्होंने इसे विदेशी ताकतों द्वारा भारत को अस्थिर बनाने का प्रयास तक करार दे दिया।
राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही कथित मानहानि विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया। वह स्वयं बोफोर्स के मामले में उलझे थे और जैल सिंह की चुनौती, वीपी सिंह की बगावत आदि का सामना कर रहे थे। वह इन बातों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे थे। वह भी नाकाम रहे। अब मोदी सरकार ने फेक न्यूज का मुकाबला करने के नाम पर मुख्यधारा के मीडिया पर लगाम कसने का कदम उठाया, बाद में नाटकीय ढंग से इस कदम को वापस ले लिया गया। हालांकि सरकार के मोर्चे पर मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। वापस ली गई प्रेस विज्ञप्ति के बाद एक समिति गठित करने की बात कही गई जो डिजिटल मीडिया के संचालन के मानक तय करे। दलील यह दी जा रही है कि प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया दोनों के पास भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडड्र्स अथॉरिटी के रूप में नियामक मौजूद हैं लेकिन नए डिजिटल मीडिया के पास इनका अभाव है। इसे स्वायत्त संस्थान के रूप में काम नहीं करने दिया जा सकता। तीन उदाहरणों का नियम पत्रकारिता के सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है। अगर तीन तथ्य एक ही बात कह रहे हों तो इससे उस बात को साबित माना जा सकता है। यानी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ताकतवर सरकारों के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कुछ तो ऐसा होता है कि वे मीडिया पर ही नकेल कसने लगती हैं। ऐसा क्यों? शायद वे अपने अगले कार्यकाल की निश्चिंतता को लेकर सामने आई अनिश्चितता से उभरी असुरक्षा को संभाल न पाते हों।
सन 1975 के आरंभ से ही इंदिरा गांधी के पराभव की शुरुआत हो गई थी जब मुद्रास्फीति की दर 20 फीसदी से ज्यादा हो गई थी और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया था। यह मानना गलत होगा कि मतदाताओं ने उन्हें प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने की सजा दी। अगर उन्होंने जबरन नसबंदी जैसी बड़ी गलती न की होती तो आपातकाल के दौरान देखा जा रहा अनुशासन बहुत लोकप्रिय था। परंतु उनकी हार और जिन प्रतिद्वंद्वियों को उन्होंने जेल में डाला था उनके उभार के बाद एक तरह का माहौल तैयार हुआ जहां आम जनता के विचारों में सेंसरशिप की कमी को पहचाना गया और प्रेस की स्वतंत्रता की बात उभरकर सामने आई। एक ऐसे देश में जहां प्रेस की आजादी को लेकर कोई विशिष्ट कानून नहीं था वहां यह एक अहम बदलाव था। सर्वोच्च न्यायालय जो आपातकाल को लेकर अपनी आश्वस्ति के चलते पश्चाताप के भाव में था, उसने भी आने वाले दशकों में इस सामाजिक भावना को कानूनी जामा पहनाया। प्रेस पर नियंत्रण का इंदिरा गांधी का दांव उलटा पड़ गया था।
राजीव ने भी अपने पराभव का दोष मीडिया पर डालना चाहा। उनकी मां की तरह उनका दांव भी उलटा पड़ गया। देश के तमाम वरिष्ठ संपादक और मालिकान अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी भुलाकर राजपथ पर एक साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। यह एकता आपातकाल के दौरान देखने को नहीं मिली थी। राजीव पीछे हट गए लेकिन इस दौरान मीडिया की नई एकता और आजादी को लेकर उसकी प्रतिबद्धता सामने आ चुकी थी। मीडिया के दमन की ऐसी हर कोशिश के बाद वह मजबूत होकर उभरा। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या एक बार फिर तीन उदाहरणों वाला नियम सच साबित होगा और नाराज सरकार मीडिया पर लगाम कसने में नाकाम होगी?
भाजपा सरकार के सामने अंतिम वर्ष में कई चुनौतियां हैं लेकिन पिछली दो सरकारों के समान वह अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही। भारतीय मीडिया का स्वरूप बहुत बड़ा है। वह लोकप्रिय, ताकतवर, अमीर और विविधतापूर्ण है। पहला, हम जिस सामाजिक तानेबाने की बात कर रहे थे वह अवश्य कमजोर हुआ है। दूसरा, मीडिया बहुत ज्यादा बंटा हुआ है। वैचारिक मतभेद तो पहले भी थे लेकिन अब यह अंतर मंच का भी है। सत्ता प्रतिष्ठान इसकी बारीक दरारों की पड़ताल कर रहा है। एक बार यह दरार चौड़ी हुई तो तगड़ा झटका लगना तय है।
जब सरकार कहती है कि प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के पास अपना नियमन है डिजिटल के पास नहीं, तो इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। उसका इरादा मीडिया समुदाय को बांटने का है। उसे कामयाबी मिलेगी या नहीं यह अलग बहस का विषय है। बड़े मीडिया घराने जो प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल तीनों में काम कर रहे हैं उनको लग सकता है कि वे इससे प्रभावित नहीं होंगे। कई पारंपरिक मीडिया घरानों को लगता है कि नए डिजिटल माध्यम उनको भ्रष्ट, अक्षम, समझौतापरक संस्थानों के रूप में चित्रित करते हैं।
वहीं डिजिटल माध्यमों में से अनेक का मानना है कि इंटरनेट का नियमन संभव नहीं है इसलिए सरकार इसमें दखल न ही दे तो बेहतर। परंतु हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सरकार चाहे तो एक अधिसूचना जारी करके लाइसेंसिंग कर सकती है या इससे भी खराब स्थितियां तैयार कर सकती है। इंटरनेट कोई संप्रभु गणराज्य नहीं है और वैश्विक स्तर पर भी इसके नियमन का मिजाज बना हुआ है। जब बात इसका मुकाबला करने की आएगी तो हमारे साथ वही पारंपरिक मीडिया होगा जिसे कुछ लोग नकारते हैं। इसका उलटा भी सही है। बिना राजस्व मॉडल के काम कर रहे इन माध्यमों की अवमानना भी खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली बात है।
बीता सप्ताह जम्मू कश्मीर में कठुआ और उत्तर प्रदेश में उन्नाव से आ रही दिल दुखा देने वाली कथाओं से भरा रहा। दोनों स्थानों पर राजनीतिक प्रतिष्ठान के दंभ ने न्याय की राह रोकी। यहां हर तरह के मीडिया के प्रयास से ही हवा का रुख बदला। समय की मांग पर इन्हें साथ आना होता है। तब कोई भेद नहीं रह जाता। हम प्राय: असहमत होते हैं, लड़ते हैं और एक दूसरे का आकलन भी करते हैं। हम पत्रकार ऐसे ही होते हैं (माफ कीजिएगा देवेगौड़ा, आपका रूपक इस्तेमाल कर रहा हूं)। परंतु प्रेस की आजादी पर हमला होने पर ऐसा नहीं रहता। यहां सीधा गणित है कि या तो एकजुट होकर अपनी आजादी बचाएं या फिर टुकड़ों में दंडित हों। इसलिए दूसरों की पत्रकारिता चाहे जितनी बुरी लगे, हमें उन पर फैसला नहीं देना चाहिए। हम अपनी आजादी तभी बचा सकते हैं जब हम अपने प्रतिद्वंद्वियों और वैचारिक विरोधियों तक के लिए लड़ें।
मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यह बात कह रहा हूं जो आपातकाल के दौर में पत्रकारिता का छात्र था और जो अब मीडिया की तीनों धाराओं में काम कर रहा है। हम पत्रकारों को अपने तमाम नए पुराने संस्थानों को मजबूत बनाना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम आपसी सहमति से काम करें और एकजुट होकर अपने सिद्धांतों की रक्षा करें। इससे कोई फर्क नहीं पडऩा चाहिए कि हम कहां और किस धारा में पत्रकारिता करते हैं।
[शेखर गुप्ता]
(साभार: बिजनेस स्टैण्डर्ड & फोटो - shutterstock)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
swatantrabharatnews.com






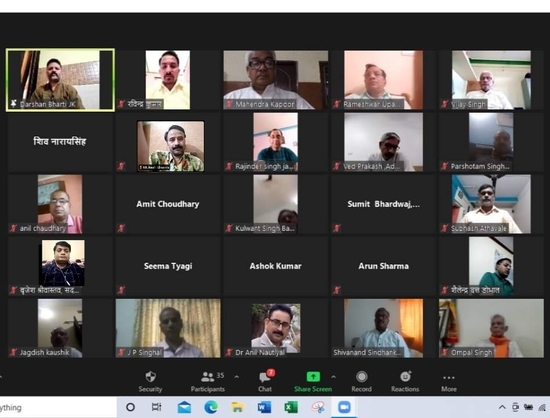

10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)
