
विशेष: मजदूर दिवस: राष्ट्र के विकास की धुरी है श्रमिक
मनुष्य की वास्तविक संपत्ति का आधार है 'श्रम'
श्रमिक शब्द 'श्रम' से बना है। श्रम का मतलब होता है - 'मेहनत'। मेहनत दो तरीके की होती है: 1.शारीरिक मेहनत और 2. मानसिक मेहनत।
शारीरिक या मानसिक मेहनत करके आजीविका चलाने वाले व्यक्ति को 'श्रमिक' कहते है। अर्थशास्त्र में 'श्रम' का अर्थ है- शारीरिक श्रम। इसमें मानसिक कार्य भी शामिल हैं।
एस. ई. थॉमस के अनुसार 'श्रम' शरीर या मन के सभी मानवीय प्रयासों को दर्शाता है, जो की इनाम की उम्मीद में किया जाते हैं"। कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, डॉक्टर, अधिवक्ता, अधिकारी और शिक्षक व अन्य सभी की सेवाएं 'श्रम' में शामिल हैं। बगीचे में माली के काम को विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के काम को 'श्रम' कहा जाता है, क्योंकि वह इसके लिए आय प्राप्त करता है।
शिक्षक द्वारा अपने बेटे को पढ़ाया जाना, एक डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज करना, एक माँ द्वारा अपने बच्चे को पालना, ये सारे कार्य आय अर्जित करने के लिए नहीं किये गए हैं। अतएव अर्थशास्त्र में इन गतिविधियों को श्रम नहीं माना जाता है। शारीरिक या मानसिक कार्य जो आय प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु आनंद और ख़ुशी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो 'श्रम' की श्रेणी में नहीं आता है अर्थात वो श्रम नहीं है।
जिस प्रकार मछली का सम्बन्ध पानी से है, उसी तरह श्रमिक का सम्बन्ध श्रम से है। मछली बगैर पानी के जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार श्रमिक बगैर श्रम के जीवित नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य । श्रम आजीविका का साधन है। जिस पर श्रमिक निर्भर रहता है। मजदूर शारीरिक श्रम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। वहीँ शिक्षित वर्ग मानसिक श्रम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है द्य मजदूर और शिक्षित वर्ग दोनों श्रमिक हैं। एक शारीरिक श्रम पर निर्भर है तो दूसरा मानसिक श्रम पर। अतएव बिना श्रम के श्रमिक की बात करना निरर्थक है। श्रम है तो श्रमिक है।
श्रम किया जाता किसी कार्य को करने के लिए। यही कार्य कर्म कहलाता है। अच्छी दिशा में की गई मेहनत अच्छा कर्म कहलाता है। गलत दिशा में की गई मेहनत बुरा कर्म कहलाता है।
यदि व्यक्ति द्वारा किया गया श्रम राष्ट्रहित में है तो कर्म अच्छा है। कहने का तात्पर्य श्रम और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत (श्रम) करता है तो वह एक सफल व्यक्ति बनता है। व्यक्ति द्वारा किया गया श्रम ही मानव कर्म कहलाता है।
मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य प्राणियों की मानसिक शक्ति की अपेक्षा मनुष्य की मानसिक शक्ति अत्यधिक विकसित है। यदि संत जनो की माने तो मनुष्य वह है जो इस संसार को धर्मशाला समझे और अपने आप को उसमे ठहरा हुआ यात्री। इस प्रकार कर्म करते हुए वह कर्म के बंधनो में न ही बंधेगा और न ही उसमे विकार भाव उत्पन्न होंगे। श्रम मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। बिना श्रम के जीवन निरर्थक है अर्थात श्रम ही जीवन है। हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थ भगवदगीता में वर्णित है। मूल श्लोकः
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।2.47।।
भावार्थ है, कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है। फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो।।
कर्म जीवन है। आलस्य मृत्यु है। श्रम न करने से जीवन नर्क बनता है। श्रम करने से जीवन स्वर्ग बनता है। श्रम से मानव फरिश्ता कहलाता है।श्रम न करने से मानव शैतान कहलाता है। कहा भी गया है कि, "खाली दिमाग शैतान का घर" श्रम लक्ष्य का आधार है। श्रम करने से मन प्रसन्न होता है। श्रम से शरीर स्वस्थ रहता है। समाज में सम्मान का कारक है श्रम। श्रम करने से व्यक्ति सफल होता है। श्रम करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत्र बनता है। आलस्य से जीवन की दौड़ में लोग पिछड़ जाते है द्य कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी ही होगी जो इस प्रकार है। खरगोश तेज गति से दौड़ता है। वह अपने तेज चलने पर बहुत गर्व करता है। सबको मालूम है कि, कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है। दोनों की दौड़ होती है- कछुआ लगातार चलता रहता है। परिणामस्वरूप कछुआ गंतव्य पर पहले पहुँच जाता है। किन्तु खरगोश आलस्य के कारण पिछड़ जाता है। श्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। मेहनत के बल पर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए। अटल विहारी वाजपई प्रधानमंत्री हुए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो, श्रम के बल पर शिखर पर पंहुचे।
श्रम से ही लोग स्वतंत्र लेखक, स्तम्भकार, पत्रकार, जज (न्यायाधीश), आई ई एस, आई ए एस, वैज्ञानिक, आदि बनकर राष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं। होनहार और मेधावी छात्र अपने आलस्य के कारण कुछ नहीं कर पाता है। किसी ने क्या खूब कहा है - कड़ी मेहनत लोगों के चरित्र को उजागर करती है- श्रम, राष्ट्र की उन्नति के लिए अनिवार्य है। श्रम, सफलता का सूचक है। कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता अर्जित की जा सकती है। मनुष्य जितना श्रम करता है, उतनी ही उन्नति कर लेता है।
हमारे देश में कई उद्योग घराने हैं- टाटा और बिरला के नाम को कौन नहीं जानता। उन्होंने साम्रज्य स्थापित कर रखे है। यह सब उनके श्रम का ही परिणाम है। बिरला मंदिर देश के कई बड़े शहरों में देखने को मिलते है। बिरला ने धन भी कमाया है और दान भी किया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने श्रम के कारण ही प्रधानमंत्री बन पाए। आइस्टीन ने श्रम किया और वे विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए।
श्रम से व्यक्ति का निर्माण होता है। श्रम से वह नेता बनता है। श्रम से वह अभिनेता बनता है। फ़िल्मी अभिनेताओं का जीवन बहुत ही आकर्षक लगता है। हर कोई अभिनेता बनना चाहता है लेकिन ये सरल नहीं है। एक अभिनेता का जीवन घोर तपस्या का परिणाम का फल होता है। साधू और सन्यासी श्रम एवं तपस्या के बल पर ही ईश्वर का दर्शन करते हैं। ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, तुलसीदास बाल्मीकि, वेद व्यास, भगवान महावीर, महात्मा गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव आदि का जीवन श्रम से परिपूर्ण था। श्रम के बिना जीवन संभव नहीं है। मानसिक श्रम हो या शारीरिक श्रम, दोनों श्रम राष्ट्र के निर्माण में अहम् भूमिका निभाते हैं।
राष्ट्रीय विकास के दो छोर हैं। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। इन्ही दो छोर पर राष्ट्र का विकास टिका हुआ है। श्रमिकों के बिना किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता है और न ही कोई उद्योग कार्य कर सकता है। श्रमिकों के बिना देश अपाहिज सा ही है।
श्रमिक दिवस को 'मई डे' के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्यादातर 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 ई को अमेरिका के शिकागो की हेय मार्केट से हुई थी। वहाँ के मजदूरों ने कार्य करने के सीमा को 10 - 12 घंटे से हटाकर 8 घंटे करने के लिए हड़ताल की थी। उस दिन बम बिस्फोट से कई मजदूरों की मृत्यु हो गयी तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से सात लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अंत में मजदूरों की माँग मान ली गई थी। 1923 में भारत में मजदूर दिवस पहली बार चैन्नई में मनाया गया था। इसे मेरठ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मजदूर दिवस को मनाने का हर देश का अपना अलग तरीका है लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि, मजदूरों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना और उन्हें पूर्ण सम्मान और हक़ दिलाना है।
मजदूर दिवस को एक उत्सव की तरह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान के अन्तर्गत वे समस्त अधिनियम आते हैं जो श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभों, बीमारी, प्रसूति, रोजगार सम्बन्धी आघात, प्रॉविडेण्ट फण्ड, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। इस श्रेणी में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी प्रॉविडेण्ट फण्ड अधिनियम, 1952; न्यूनतम भृत्ति अधिनियम, 1948; कोयला- खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1947; भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम, 1934; खदान अधिनियम, 1952 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में वर्तमान में 128 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू हैं जिसमें से वर्ष २०१६ से भारत में कई श्रम कानूनों को संशोधित/ निष्प्रभावी बनाया गया है जो श्रमिकों के हित में नहीं हैं और श्रमिक संघ इनको श्रम बिरोधी बताते हुए बिरोध कर रहे हैं।
वास्तव में श्रम विधान सामाजिक विधान का ही एक अंग है। श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिये बनाये गये विधान, सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं।
औद्योगीकरण के प्रसार, मजदूरी, अर्जकों के स्थायी वर्ग में वृद्धि, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुये महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार, श्रम संघों के विकास, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, संघों - श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार, प्रबन्धकों और नियोजकों के परमाधिकारों में ह्रास तथा कई अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता बढ़ती गई है।
श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते हुये महत्व को ध्यान में रखते हुये उन्हें एक अलग श्रेणी में रखना उपयुक्त समझा जाता है। श्रम विधान में व्यक्तियों या उनके समूहों को श्रमिक या उनके समूह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक श्रम विधान के कुछ महत्वपूर्ण विषय है। मजदूरी की मात्रा, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी से कटौतियां, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टी, कार्य की भौतिक दशायें, श्रम संघ, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, स्थायी आदेश, नियोजन की शर्ते, बोनस, कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति हितलाभ एवं कल्याण निधि आदि है।
श्रम कानून के उद्देश्य: श्रम विधान के अग्रलिखित उद्देश्य हैं:
1. औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना।
2. मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना।
3. विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुये महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार को देखते हुये स्थानीय परिदृश्य में लागू कराना।
4. श्रम संघों का विकास करना।
5. श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना।
6. संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना।
7. प्रबन्धकों और नियोजकों के परमाधिकारों में ह्रास तथा कई अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता को बढ़ाना।
घर से लेकर उद्योग तक के निर्माण के लिए मजदूर आवश्यक है। वह दिन रात कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मजदूर दिवस के दिन 80 देशों में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। मजदूरों को परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए सप्ताह में एक अवकाश उनके उत्साह को दुगना करता हैं।
फ़िलहाल अभी देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉक डाउन की स्थिति है जिसमे सभी लोगों को परिवार के साथ रहने का भरपूर मौका मिल रहा है। परन्तु साथ ही कामगारों / श्रमिकों के सामने रोजगार से लेकर कई समस्याएं कड़ी हो गयी हैं। सरकार को चाहिए कि, श्रमिकों के अधिकारों का शोषण न होने दें। श्रमिकों की काम करने की अवधि आठ घंटे है और कोई भी उद्योगपति उनसे इससे ज्यादा कार्य नहीं करवा सके। मजदूर जहाँ कार्य करते है वहाँ उनका बीमा और मैडिकल होना और उनके परिवार की सुरक्षा का होना सुनिश्चित होना चाहिए। कोरोना (कोविड-19) महामारी में मजदूरों की स्थिति पर सरकार नजर रखी है और सरकारी खजाने से उनकी सहायता की जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री - योगी आदित्य नाथ ने उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे मजदूरों को अपने प्रदेश में वापस लाने का आदेश जारी किया है। हालांकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का देरी से उठाया गया कदम है फिर भी सराहनीय कदम है। राष्ट्र के विकास की नींव श्रम से ही रखी जाती है इसलिये सरकार के सामने श्रमिकों के काम को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है।
[उपरोक्त लेख मई दिवस के उपलक्ष में डॉ शंकर सुवन सिंह, स्तम्भकार, चिंतक व असिस्टेंट प्रोफेसर- सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (शुएट्स), नैनी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) हैं तथा संपादक द्वारा सम्पादित किया गया है।]
swatantrabharatnews.com



.jpg)
.jpg)
.jpg)
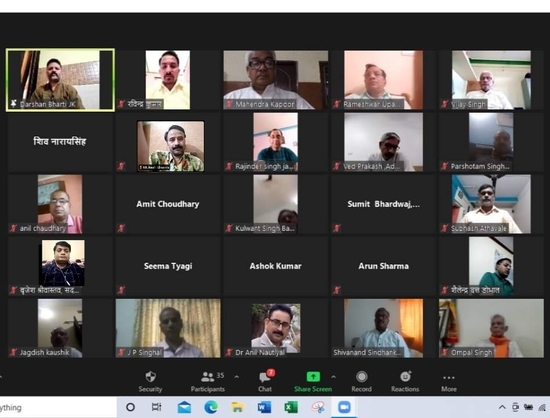

10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)
