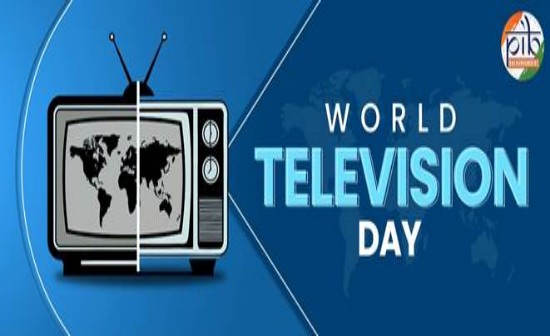
विश्व टेलीविज़न दिवस 2025: PIB हेडक्वार्टर्स
पूरे भारत में 23 करोड़ घरों तक पहुंच
नई दिल्ली (PIB): PIB हेडक्वार्टर्स ने "विश्व टेलीविज़न दिवस 2025" के अवसर पर एक विशेष प्रस्तुति प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया है कि, भारत का टेलीविज़न नेटवर्क पूरे भारत में 23 करोड़ घरों तक पहुंच बनाई है !
"विश्व टेलीविज़न दिवस 2025" के अवसर पर एक विशेष प्रस्तुति":
प्रमुख बिंदु
|
परिचय
विश्व टेलीविज़न दिवस प्रति वर्ष 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से 1996 में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यह दिन हमें बताता है कि टेलीविज़न लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने एवं जनता की राय को प्रभावित करने, और संचार तथा और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी माध्यम है।
भारत में 23 करोड़ से ज़्यादा घरों में टेलीविज़न हैं और लगभग 90 करोड़ दर्शक इसे देखते हैं। यह दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसके सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्क, प्रसार भारती की देखरेख में मनाया जाता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी की गतिविधियां और जन संपर्क कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा संचार, विकास के संदेश फैलाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में टेलीविज़न की स्थायी भूमिका है।
टेलीविज़न भारत में सूचना और मनोरंजन तक पहुँच के लिए सबसे ताकतवर प्लेटफ़ॉर्म में से एक बना हुआ है। यह लाखों घरों को जोड़ता है और जन जागरूकता और भागीदारी शासन के उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
|
क्या आप जानते थे? भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट (एमएंड ई) क्षेत्र ने 2024 में अर्थव्यवस्था में ₹2.5 ट्रिलियन का योगदान दिया और 2027 तक इसके ₹3 ट्रिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है। अकेले टेलीविज़न और प्रसारण क्षेत्र ने 2024 में लगभग ₹680 बिलियन कमाए। इस क्षेत्र की वृद्धि डिजिटल विस्तार, 4K ब्रॉडकास्टिंग, स्मार्ट टीवी, 5G और OTT प्लेटफॉर्म से हो रही है, जो 60 करोड़ से ज़्यादा उपयोक्ताओं को सेवा दे रहे हैं। |
भारत में टेलीविज़न की वृद्धि
भारत में टेलीविज़न सीमित प्रायोगिक सेवा से दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्क में से एक बन गया है। यह संचार प्रौद्योगिकी, जन संपर्क और डिजिटल नवाचार में देश की तरक्की को दिखाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मार्गदर्शन में भारत में टेलीविज़न की यात्रा देश के सामाजिक- आर्थिक विकास को दिखाती है जिसमें 1950 के दशक में सामुदायिक शिक्षा प्रसारण से लेकर आज पूरी तरह से डिजिटाइज़्ड, मल्टी-चैनल माहौल तक का विकास शामिल है। नीचे दिए गए चरणों में इस बदलाव को दिखाया गया है। इनमें आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नीति संबंधी प्रमुख उपलब्धियां और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति को दिखाया गया है।
प्रायोगिक और बुनियादी चरण (1959–1965)
भारत में टेलीविज़न प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) ने शुरू किया था। यह सेवा यूनेस्को के साथ मिलकर शुरू की गई थी ताकि शिक्षा और सामुदायिक विकास में टेलीविज़न की भूमिका का पता लगाया जा सके। आरंभ में, प्रसारण दिल्ली के आस-पास छोटे से दायरे तक ही सीमित थे, जिसमें विद्यालय शिक्षा और ग्रामीण विकास पर केंद्रित कार्यक्रम शामिल थे।
विस्तार और संस्थानीकरण (1965-1982)

नियमित दैनिक ट्रांसमिशन 1965 में शुरू हुआ, जिससे दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अंदर समर्पित टेलीविज़न सेवा थी। इस दौरान, टेलीविज़न तेज़ी से सीमित प्रयोग से बढ़ते हुए सार्वजनिक सेवा माध्यम में बदल गया। मुंबई (1972), श्रीनगर, अमृतसर, और कलकत्ता (1973–75), और चेन्नई (1975) जैसे बड़े शहरों में नए टेलीविज़न केंद्र बनाए गए। इससे कवरेज बढ़ा और राष्ट्रीय प्रसारण अवसंरचना मज़बूत हुई। दूरदर्शन भारत में प्रसारण परिदृश्य में अहम पहलू के तौर पर उभरा। इससे इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय माध्यम के तौर पर टेलीविज़न के तेज़ी से विस्तार का पता चलता है।
इस दौर का महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1975-76 में इसरो और नासा का सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (एसआईटीई) था, जो दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह-आधारित शिक्षा प्रयोग में से एक था। एसआईटीई के तहत, नासा के ATS-6 सैटेलाइट ने छह राज्यों के 20 जिलों के लगभग 2,400 गांवों में शिक्षा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया, जबकि इसरो ने ग्राउंड सिस्टम दिए और एआईआर ने प्रोग्राम प्रोडक्शन को प्रबंधन किया। ये कार्यक्रम खेती, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित थे — जिसने भारत में उपग्रह-आधारित विकास संचार की नींव रखी।
दूरदर्शन ने मनोरंजन से आगे बढ़कर समाचार, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सामुदायिक शिक्षा और शैक्षिक संपर्क में अपने दायरे का विस्तार किया। नेटवर्क ने विद्यालय शिक्षा, ग्रामीण विकास और जागरूकता बढ़ाने में व्यवस्थित प्रसारण शुरू किए, जिससे यूजीसी के उच्च-शिक्षा प्रसारण और सीईसी के पाठ्यक्रम-आधारित कार्यक्रम प्रोग्रामिंग जैसी भविष्य की राष्ट्रीय पहल के लिए मंच तैयार हुआ।
इस दौर में देश भर में प्रमाणिक, संतुलित समाचार और सार्वजनिक सूचना देने में दूरदर्शन की बढ़ती भूमिका भी दिखाई दी, क्योंकि सार्वजनिक प्रसारक मनोरंजन से आगे बढ़कर सामाजिक विकास के साधन के रूप में विकसित हुआ। क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों ने स्थानीय भाषा में कार्यक्रम बनाने की प्रक्रिया को मज़बूत किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सका। टेलीविज़न केंद्र और रीजनल प्रोडक्शन यूनिट के बढ़ने के साथ, दूरदर्शन ने स्थानीय भाषा में कार्यक्रम बनाने की प्रक्रिया को मज़बूत किया और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया।
1980 के दशक की शुरुआत तक, भारतीय टेलीविज़न की संस्थागत नींव मज़बूती से बन चुकी थी। इसमें देशव्यापी नेटवर्क, विकास पर आधारित कार्यक्रमों की सोच, और रंगीन प्रसारण और नेशनल कवरेज सहित बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी क्षमता शामिल हैं जिसने अगले चरण के विस्तार को आगे बढ़ाया।
रंगीन टेलीविज़न और नेशनल कवरेज (1982–1990)
1982 में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत नई दिल्ली में एशियन खेलों के साथ हुई। यह भारत के प्रसारण इतिहास में मील का पत्थर थी। इस अवधि में दूरदर्शन के तहत टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का तेज़ी से विस्तार हुआ, जिससे ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों तक पहुँच बढ़ी। 1990 तक, दूरदर्शन का नेटवर्क भारत की लगभग 70% आबादी और 80% भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच गया। 1980 के दशक में, दूरदर्शन ने अपने रीजनल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स की भूमिका को भी बढ़ाया जिन्हें दूरदर्शन केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम बनाते और प्रसारण करते हैं, जिससे नेशनल प्रसारण में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता मज़बूत हुई।
मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
- उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए समर्पित चैनल
- आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकसित किए गए कार्यक्रम
- अधिकतम लचीलेपन के लिए रिपीट स्लॉट के साथ लगातार प्रसारण
- DD फ्री डिश सहित DTH प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता
यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों तरह के विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के मिले, जिससे भारत की मिश्रित शिक्षा पारिस्थितिकी और अधिक मज़बूत हो!
श्रोता-दर्शक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
टेलीविजन भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला माध्यम बना हुआ है, जिसमें सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट चैनल्स की अच्छी पहुंच है। 31 मार्च 2025 तक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में 918 प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों (अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग या दोनों के लिए) को अनुमति दी थी। इनमें से, भारत में डाउन-लिंकिंग के लिए 908 चैनल उपलब्ध थे, जिनमें से 333 पे टीवी चैनल (232SD +101HD) थे।
SD चैनल कम रिज़ॉल्यूशन और बैंडविड्थ पर वीडियो उपलब्ध कराते हैं, जबकि HD चैनल बढ़े हुए रिज़ॉल्यूशन के कारण काफी ज़्यादा पिक्चर क्लैरिटी और डिटेल देते हैं, जो खासकर बड़ी स्क्रीन पर, देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है। चैनलों की संख्या 2014 में 821 से 2025 में 918 तक बढ़ोतरी इस बात पर ज़ोर देती है कि कैसे टेलीविज़न भाषाई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सूचनात्मक माध्यम बना हुआ है।
टेलीविज़न का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है: यह कंटेंट बनाने, ब्रॉडकास्टिंग के काम और रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में रोज़गार देता है; प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में आजीविका में मदद करता है; और ग्रामीण एवं छोटे शहरों की आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं तक पहुँच देता है। टेलीविज़न की बड़ी पहुँच, भाषाई विविधता और रेगुलेटरी निगरानी भारत के मीडिया माहौल में सांस्कृतिक और आर्थिक चालक के तौर पर इसके लगातार महत्व को दिखाते हैं।
भारतीय टेलीविज़न में प्रौद्योगिकी और नवाचार
टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम डिजिटल अवसंरचना उन्नयन, प्रौद्योगिकी नवाचार और रेगुलेटरी सुधारों के ज़रिए बड़े बदलाव से गुज़र रहा है—जो सरकारी नीति और सार्वजनिक प्रसारक, प्रसार भारती के प्रयासों से चल रहा है।
टेरेस्ट्रियल ट्रांज़िशन और अवसंरचना आधुनिकीकरण
भारत में एनालॉग से डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (DTT) में बदलाव ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर पहले लगभग 88% आबादी को कवर करते थे, लेकिन इस सिस्टम में कुछ कमियाँ थीं, जैसे चैनल कैपेसिटी कम होना और पिक्चर और साउंड की क्वालिटी कम होना।
|
डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न (DTT) क्या है? DTT, पारंपरिक एनालॉग ट्रांसमिशन की जगह, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट टावरों के ज़रिए टेलीविज़न सिग्नल को डिजिटल तरीके से भेजता है। यह कई चैनल, बेहतर पिक्चर क्वालिटी और बिना केबल या सैटेलाइट लिंक के मोबाइल रिसेप्शन देता है। |
डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल और सिग्नल की क्लैरिटी बेहतर करता है। भारत का DTT नेटवर्क DVB-T2 (डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग – सेकंड जेनरेशन टेरेस्ट्रियल) स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे मोबाइल या इनडोर माहौल में भी बेहतर रिसेप्शन के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर कई टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं। फरवरी 2016 में 16 शहरों में पहले DVB-T2 डिजिटल ट्रांसमीटर चालू किए गए थे, और देश भर में 630 जगहों तक डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने की दीर्घावधि योजना है।
करीब 50 खास जगहों को छोड़कर दूरदर्शन के लगभग सभी एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर बंद कर दिए गए हैं। ये बची हुई जगहें—खासकर बॉर्डर, दूरदराज या सेंसिटिव इलाकों में—भरोसेमंद टेलीविज़न कवरेज सुनिश्चित करती हैं, जहाँ DTH या केबल कनेक्टिविटी अब भी कम हो सकती है। सीमित एनालॉग फुटप्रिंट रखने से पूरे डिजिटल ऑपरेशन में बदलाव के दौरान सेवा जारी रखने में भी मदद मिलती है, जबकि बड़े पैमाने पर इसे बंद करने से कीमती स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे 5G ब्रॉडकास्ट सर्विस जैसी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
पब्लिक फ्री-टू-एयर DTH के ज़रिए पहुंच का विस्तार करना
जिन घरों में, खासकर दूर-दराज, बॉर्डर और आदिवासी इलाकों में केबल या, टेरेस्ट्रियल कनेक्शन नहीं हैं, वहां उन तक पहुंचने के लिए प्रसार भारती के DD फ्री डिश को काफी बढ़ाया गया है। आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि अभी 6.5 करोड़ से ज़्यादा घर इस फ्री-टू-एयर DTH सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म MPEG-2 और MPEG-4 दोनों स्लॉट देता है और ई-बोली एलोकेशन के ज़रिए प्राइवेट टीवी चैनलों को आमंत्रित करता है, जो टेक्नोलॉजी अपनाने और कंटेंट में विविधता लाने के लिए सबको साथ लेकर चलने वाला तरीका दिखाता है।
|
MPEG क्या है? MPEG (मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप) डिजिटल वीडियो कम्प्रेशन के लिए वैश्विक मानकों का संदर्भ लेता है।
|
अपनी शुरुआत से ही, DD फ्री डिश ने चैनल कैपेसिटी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी है— इसके 2014 में 59 चैनलों से बढ़कर 2025 में 482 चैनल हो गए हैं, जिससे पूरे देश में नेशनल, रीजनल और एजुकेशनल कंटेंट की बड़ी रेंज तक पहुंच बढ़ गई है।
DD फ्री डिश पूरे भारत में, खासकर दूर-दराज, बॉर्डर और कम सुविधा वाले इलाकों में टेलीविज़न एक्सेस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम (DTH) प्लेटफॉर्म के तौर पर, यह नेशनल, रीजनल और एजुकेशनल कंटेंट तक भरोसेमंद पहुंच देकर दूरदर्शन के डिजिटल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को पूरा करता है। इसका इनक्लूसिव मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि जिन घरों में केबल या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वे भी देश के बदलते ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा सकें।
बदलती नियामक रूपरेखा और अनुमोदन सुधार
भारत का नियामक वातावरण ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के कन्वर्जेंस के हिसाब से बदल रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने “दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए सेवा अनुमोदन की रूपरेखा” पर सुझाव जारी किए हैं। इसमें नई कानूनी पद्धति के साथ तालमेल बिठाने के लिए ऑपरेशनल और लाइसेंसिंग ज़रूरतों को अपडेट किया गया है।
ये सुधार सरकार के मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करने, OTT सर्विसेज़ को एकीकृत करने और भारत की प्रसारण पारिस्थितिकी में सेवा की गुणवत्ता, सुगम सुलभ कराने की क्षमता और बाज़ार की निगरानी सुनिश्चित करने के इरादे को दिखाते हैं।
*****

.jpg)



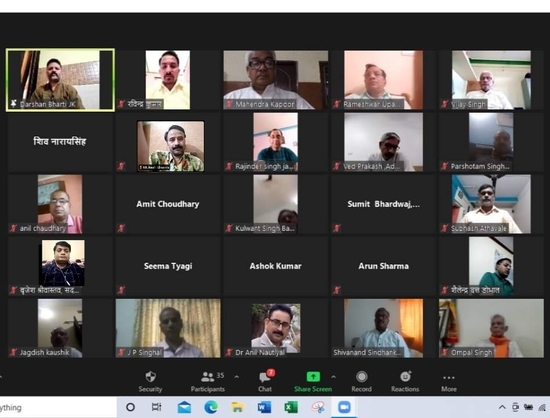

10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)
